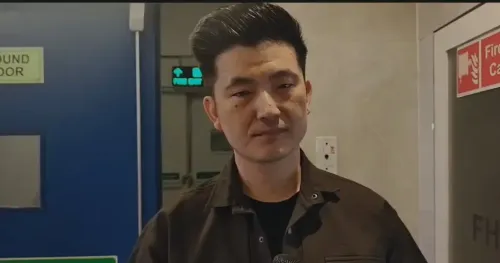क्या तपन सिन्हा ने सिनेमा की पुरानी जकड़न को तोड़ा?

सारांश
Key Takeaways
- तपन सिन्हा ने भारतीय सिनेमा में सामाजिक यथार्थवाद को प्रमुखता दी।
- उनकी फिल्में आज भी प्रासंगिक हैं।
- उन्हें 19 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं।
- उन्होंने साउंड इंजीनियर से निर्देशक बनने का सफर तय किया।
- उनकी फिल्में न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि शिक्षा भी देती हैं।
मुंबई, 14 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय सिनेमा में, खासकर बंगाली और हिंदी फिल्मों में सामाजिक यथार्थवाद, मानवतावाद और संवेदनशील कहानी कहने की नई मिसाल कायम करने वाले तपन सिन्हा के नाम से कौन अपरिचित होगा? उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो समाज को आईना दिखाती थीं, राष्ट्रीय एकता का संदेश देती थीं और दर्शकों के दिलों में स्थाई जगह बनाने में सफल रहीं। 15 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है।
2 अक्टूबर 1924 को जन्मे तपन दा को सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन के साथ भारतीय सिनेमा की चौकड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। उनका फिल्मी सफर साधारण था। साल 1946 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध न्यू थिएटर्स में साउंड इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया, जहाँ उनका वेतन मात्र 70 रुपए प्रति माह था। लेकिन यही वह स्थान था जहाँ से सिनेमा का जादू उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। 1950 में, उन्होंने ब्रिटेन के पाइनवुड स्टूडियोज में दो वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण की तकनीक सीखी। भारत लौटने के बाद उन्होंने निर्देशन की दिशा में कदम बढ़ाया, जिसमें उनकी मां और दोस्तों का सहयोग मिला।
तपन दा का रवींद्रनाथ टैगोर से गहरा लगाव था। एक दिन स्कूल में प्रिंसिपल ने टैगोर की कहानियां पढ़ीं, जिससे उनका साहित्य और संगीत के प्रति प्रेम बढ़ा। उनकी मां रवींद्र संगीत गाती थीं, जिसने उन्हें संगीत का महत्व सिखाया। इस प्रकार, तपन सिन्हा ने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज सुधार का माध्यम बनाया। उनकी फिल्में आज भी प्रासंगिक हैं।
उनकी पहली फिल्म 1954 में आई अंकुश, जो एक हाथी की कहानी पर आधारित थी। लेकिन असली पहचान उन्हें 1957 में रिलीज हुई काबुलीवाला से मिली, जो रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और बर्लिन फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार भी प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने क्षुदीतो पाषाण, अपनजन, सगीना महतो, हाटे बाजारे, सफेद हाथी जैसी यादगार फिल्में बनाईं।
तपन सिन्हा की फिल्मों की खासियत यह थी कि वे सामाजिक मुद्दों को बहुत संवेदनशीलता से उठाते थे। मजदूर अधिकार, पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक अन्याय, बच्चों की दुनिया और फैंटेसी जैसी थीम्स पर उन्होंने काम किया। 'सगीना' में दिलीप कुमार ने मजदूर नेता का किरदार निभाया। 'एक डॉक्टर की मौत' में उन्होंने वैज्ञानिक की प्रतिभा और नौकरशाही की ईर्ष्या को दर्शाया। बच्चों के लिए 'सफेद हाथी' और 'आज का रॉबिनहुड' जैसी फिल्में बनाकर उन्होंने मनोरंजन के साथ शिक्षा भी दी।
उनकी फिल्में न केवल भारत में, बल्कि बर्लिन, लंदन, मॉस्को जैसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भी सराही गईं। उन्होंने बंगाली, हिंदी और उड़िया भाषाओं में 40 से अधिक फिल्में बनाई। उनके नाम 19 नेशनल अवॉर्ड्स हैं और वर्ष 2006 में उन्हें भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला।
15 जनवरी 2009 को उन्होंने अंतिम सांस ली।