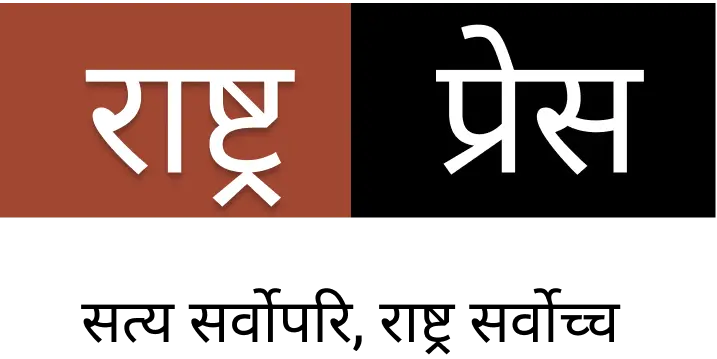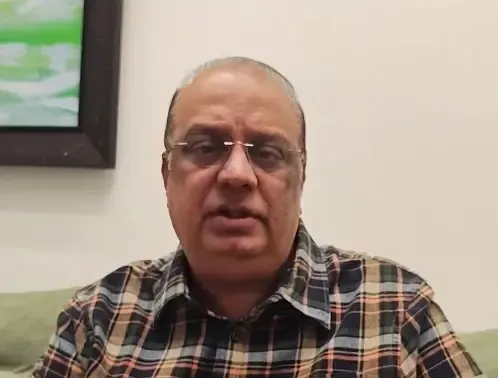क्या 40 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'आखिर क्यों' ने फेमिनिज्म को नए कलेवर में प्रस्तुत किया?

सारांश
Key Takeaways
- महिला सशक्तिकरण का नया दृष्टिकोण
- संघर्ष और आत्म-खोज की कहानी
- स्मिता पाटिल का प्रभावी अभिनय
- फेमिनिज्म की नई परिभाषा
- भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण फिल्म
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। जब प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों, शक्तिशाली संवादों और प्रभावशाली किरदारों की बात होती है, तो फिल्में यादों से मिटती नहीं हैं। ऐसी ही एक फिल्म, जो ठीक चालीस साल पहले, 7 अक्टूबर 1985 को रिलीज हुई, ने दर्शकों का दिल जीत लिया, उसका नाम है 'आखिर क्यों?' यह केवल एक ड्रामा फिल्म नहीं थी, बल्कि उस समय की बॉलीवुड फिल्मों में महिला सशक्तिकरण और भावनाओं की एक नई परिभाषा प्रस्तुत करने वाली फिल्म थी। स्मिता पाटिल ने इस फिल्म में जो भूमिका निभाई, वह आर्ट और मुख्यधारा के बीच की सीमाओं को ध्वस्त करती है और दोनों को समृद्ध करती है।
स्मिता पाटिल का नाम सुनते ही, गंभीर, शक्तिशाली और यथार्थवादी सिनेमा की छवि उभरती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत समानांतर फिल्मों से की और लगभग पांच साल तक इनमें सक्रिय रहीं। हालांकि, मुख्यधारा की फिल्मों में उनका आना आसान नहीं था, लेकिन 'आखिर क्यों' ने यह साबित कर दिया कि उनका अभिनय किसी भी प्रमुख फिल्म में गहराई और सहजता से समा सकता है। इस फिल्म में उन्होंने राजेश खन्ना, राकेश रोशन और टीना मुनीम के साथ काम किया और अपने किरदार में इतनी सहजता दिखाई कि कोई और उस पर ध्यान ही नहीं दे सका।
फिल्म की कहानी निशा शर्मा (स्मिता पाटिल) के इर्द-गिर्द घूमती है। निशा एक शादीशुदा महिला है, जो परिस्थितियों के जाल में फंसकर अपनी पहचान की खोज में निकल पड़ती है। शांत और विनम्र निशा अक्सर आंसू बहाती है, अपने पति कबीर (राकेश रोशन) से व्यवहार में बदलाव की गुहार लगाती है, लेकिन यही उसकी असली ताकत बन जाती है।
'आखिर क्यों' का पहला भाग निशा के आंसुओं में गुजरता है। दूसरे भाग में उसकी खुद से मुलाकात होती है। इस दौरान वह हमेशा पुरुषों के बीच होती है, जो उसके लिए निर्णय लेना चाहते हैं। लेकिन निशा न तो चिल्लाती है और न ही शोर मचाती है, बल्कि स्पष्टता और दृढ़ता के साथ अपने निर्णय स्वयं लेने की ताकत दिखाती है और यहीं उसका फेमिनिज्म प्रकट होता है। यह कुछ खास है, लेकिन भाषण नहीं है।
जब फिल्म देखी जाती है, तो यह लगता है कि यह उस समय की हर दूसरी फिल्म जैसी है, जहां पत्नी गिड़गिड़ाती है और जब पति नहीं मानता तो उसके खिलाफ खड़ी होने में समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि उठ खड़ी होती है। लेकिन यही 'आखिर क्यों' को एक अलग फ्रेमवर्क में तब्दील करता है। निशा अंत तक पति से बदलाव की गुहार लगाती है, लेकिन जब वह नहीं बदलता तो मजबूरी में अपने अस्तित्व की खोज में निकल पड़ती है। संघर्ष करती है, रोती है, और यही बहते आंसू उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत का प्रमाण होते हैं। यह किरदार के विकास और आत्म परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
एक ऐसा पल आता है जब कबीर हैरान होकर कहता है कि उसने कभी निशा को कुछ कहते नहीं सुना। निशा जवाब देती है कि वह पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने में व्यस्त थी। दरअसल, यह एक झटका है, क्योंकि वह यह बता रही होती है कि उसने उसे कभी परखा ही नहीं। शर्मीला और शांत होना कमजोरी का प्रतीक नहीं होता। वह यह दिखाना चाहती है कि कबीर, अपने संकीर्ण विचारों के कारण, यह समझ नहीं पाया कि महिलाएं केवल उसकी परिभाषा में नहीं बंधतीं।
निशा नामक किरदार शोर नहीं मचाता, बल्कि सादगी और सहजता के साथ अपनी बात रखता है। यह वही फेमिनिज्म है जो जोर-जबरदस्ती या आंदोलनकारी नायिका वाला नहीं है, लेकिन अपने सशक्त और संवेदनशील स्वरूप में उतना ही प्रभावी और असरदार है।